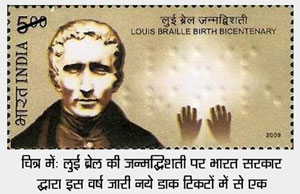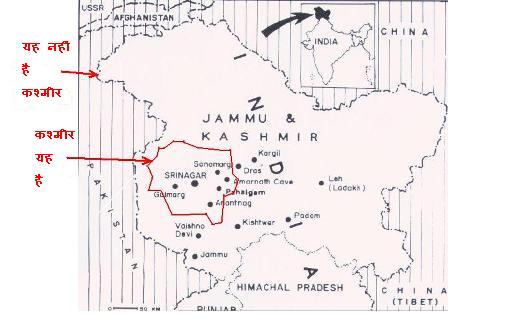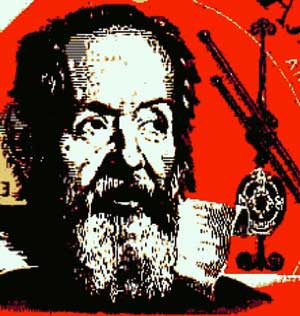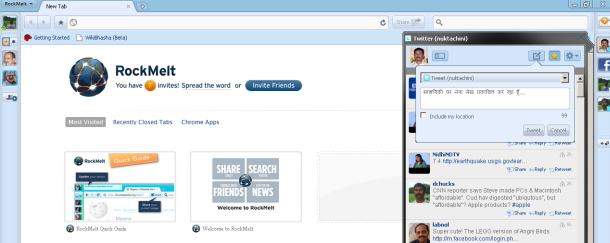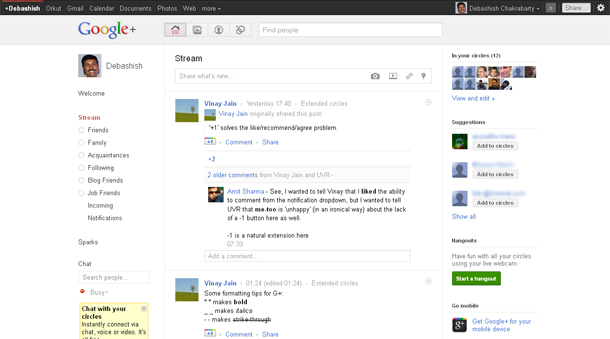2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी वर्ष घोषित किया गया है। ठीक चार सौ साल पूर्व प्रसिद्ध खगोलशास्त्री गैलिलियो गैलीली ने दूरबीन द्वारा अपनी जिज्ञासु आंखों से अंतरिक्ष की टोह ली थी।
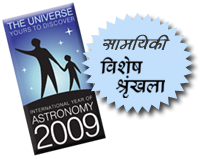 आज खगोल विज्ञान ने हमारे ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को हमारे लिए समझना आसान कर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही पर्याप्त है? अक्सर लोग खगोल विज्ञान को गोपनीय विज्ञान मानते हैं जिसकी विज्ञान के विकास में कोई बड़ी भूमिका नहीं हो सकती। जहाँ दुनिया के इतने सारे देशों में असंख्य लोग गरीबी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं वहाँ दूरबीनों, वेधशालाओं एवं खगोलीय अनुसंधान में भारी निवेश को न्यायोचित कैसे ठहराया जाये?
आज खगोल विज्ञान ने हमारे ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को हमारे लिए समझना आसान कर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही पर्याप्त है? अक्सर लोग खगोल विज्ञान को गोपनीय विज्ञान मानते हैं जिसकी विज्ञान के विकास में कोई बड़ी भूमिका नहीं हो सकती। जहाँ दुनिया के इतने सारे देशों में असंख्य लोग गरीबी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं वहाँ दूरबीनों, वेधशालाओं एवं खगोलीय अनुसंधान में भारी निवेश को न्यायोचित कैसे ठहराया जाये?
धनोपार्जन
खगोल विज्ञान में भारी निवेश को सिर्फ आर्थिक आधार पर तोला जाए तो बहुत से यदि विकासशील देशों (और शायद अन्य मुल्कों से भी) से यह गायब ही हो जाए। लेकिन सौभाग्यवश इस मामले में दक्षिण अफ्रीका का अनुभव हमें यह दिखाता है कि खगोल विज्ञान में निवेश न सिर्फ हमें बड़ा आर्थिक लाभ पहुँचा सकता है बल्कि इसके बहुत से सामाजिक लाभ भी संभव हैं।
साउथ अफ्रीकन लार्ज टेलिस्कोप (SALT) में दक्षिण अफ़्रीका के निवेश ने देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़े उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है जहाँ स्थानीय उद्योग ने ही दूरबीन के साठ प्रतिशत से ज्यादा कल-पुर्जों का उत्पादन किया है।
इस निवेश ने न केवल रोजगार पैदा किये बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। SALT के खुलने के पहले साल में ही सदरलैंड जैसे छोटे शहर, जहाँ यह दूरबीन स्थापित की गई है, में आने वाले पर्यटकों की संख्या कुछ सौ लोगों से बढ़कर 13,000 हो गयी। परिणामस्वरूप, अतिथि-गृह, कैफे, और पर्यटन संबंधी अन्य व्यवसायों में काफी वृद्धि दर्ज की गयी। SALT कोलैटरल बेनीफिट्स प्रोग्राम (SCBP), ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खगोल-पर्यटन कार्यक्रम का विकास किया। अब तो बड़ी संख्या में दक्षिण अफ्रीकी कंपनियाँ भी खगोल विज्ञान में रुचि को भुनाने में व्यस्त हैं और शौकिया दूरबीनों की मदद से देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं।
नामीबिया में भी स्थानीय लोगों अंतरिक्ष विज्ञान में नयी रुचि का लाभ उठा रहे हैं जो गाम्सबर्ग दर्रे में लगाए गये हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम (HESS) से जागृत हुई। यह उच्च क्षमता वाली दूरबीनों की एक प्रणाली है जिससे गामा-किरणों की जाँच की जाती है। उदाहरण स्वरूप इस क्षेत्र के कुछ किसानों ने भी पर्यटकों के लिए अपने बागानों में शौकिया खगोलविदों के लिये छोटी दूरबीनों की स्थापना की है। खगोल विज्ञान का विकास और प्रसार औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास की भी शुरुआत करता है – HESS परियोजना के लिए बनाये गये बहुत से जटिल फास्ट स्विचिंग यंत्रों का व्यवसायिक स्टेरेलाईज़ेशन प्रणालियों के लिये भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इनसे ओजोन बनता है जो एक तेज़ निस्संक्रामक (disinfectant) है।
जनसामान्य की भागीदारी
खगोल विज्ञान को विकास के लिए उत्प्रेरक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है जनसामान्य में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास एवं उसमें लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना। विश्व की बहुत सी संस्कृतियों में खगोल विज्ञान का एक लंबा स्थानीय इतिहास रहा है जिससे हमें लोगों के बीच ब्रह्मांड की आधुनिक समझ को पहुँचाने का रास्ता और भी सुगम हो जाता है।
SALT: दक्षिणी गोलार्द्ध की सबसे विशाल ऑप्टिकल दूरबीन

दक्षिण अफ्रीका के अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र कारू में स्थित साउथ अफ्रीकी लार्ज टेलिस्कोप (SALT) लगभग दस मीटर (~33 फीट) व्यास की आप्टिकल दूरबीन है। SALT दक्षिणी गोलार्द्ध में सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन है। यह उत्तरी गोलार्द्ध स्थित दूरबीनों की पहुँच से बाहर खगोलीय पिंडों से होते विकिरण का विश्लेषण कर सकती है। 10 नवंबर 2005 को राष्ट्रपति थाबो मबेकी ने आधिकारिक रूप से दूरबीन का उद्घाटन किया था। SALT के पहले दस साल के खर्च के लिये दक्षिण अफ्रीका से कुल 360 लाख डॉलर का लगभग एक तिहाई पैसे दिये हैं, शेष राशि जर्मनी, अमरीका, ब्रिटेन व न्यूजीलैंड जैसे सहयोगी देशों ने वहन की है।
दक्षिण अफ्रीका की वेधशालाओं ने हमेशा से लोगों के बीच वैज्ञानिक समझ पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। SCBP के कार्यक्रमों ने — तारों के अवलोकन से लेकर व्याख्यान एवं भाषणों के आयोजन तक — सदरलैंड के निवासियों के साथ संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नियमित प्रेस विज्ञप्तियाँ इसे राष्ट्रीय समाचारपत्रों की सुर्खियों में बनाये रखने का महत्वपूर्ण काम करती है, जबकि पोस्टर एवं स्मारक चिन्ह इत्यादि लोगों की दिलचस्पी बनाये रखते हैं तथा उनका ज्ञानवर्धन करते हैं।
इस तरह की प्रमुख परियोजना वास्तव में एक प्रेरणा-स्रोत का काम करती हैं। दक्षिण अफ्रीका के बहुत से युवक युवतियां अब SALT परियोजना का हिस्सा बनना चाहते हैं जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। SALT अब विद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है जिससे गणित, विज्ञान एवं अन्य तकनीकी विषयों की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने में सहायक सिद्ध हो रही है। जो खगोल विज्ञान हमेशा से एक उत्सुकता एवं जिज्ञासा का विषय रहा है उसी को माध्यम बनाकर हम अपनी संस्कृति में सीखने-सिखाने का प्रभावी माहौल तैयार कर सकते हैं।
बड़े बजट वाली खगोलीय परियोजनाएँ शिक्षा के लिए धन जुटाने का एक बड़ा माध्यम सिद्ध हो सकती हैं। SCBP द्वारा शिक्षकों एवं अन्य लोगों के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करती रहती है। इनमें दूरबीन, स्पेक्ट्रोस्कोप इत्यादि बनाने के प्रशिक्षण से लेकर मौसम, चंद्र एवं सूर्यग्रहण इत्यादि जैसे खगोलीय अवधारणाओं की व्याख्या की जाती है। संस्था द्वारा विज्ञान क्लब चलाना, शैक्षणिक सामग्री का वितरण एवं खगोल विज्ञान तथा भौतिकी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का संयोजन करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान वर्ष में हम वंचित क्षेत्रों में शिक्षकों एवं छात्रों को अभ्यास पुस्तिकाओं, पोस्टरों खेल-सामग्री, एवं कार्टून आदि का वितरण कर एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर हम लोगों के बीच और जागरूकता पैदा कर सकते हैं। एक अफ्रीकी संगठन के लिये खगोल विज्ञान के माध्यम से शिक्षा के विस्तार की यह शुरुवाती सीढ़ी सिद्ध हो सकती है।
कौशल का निर्माण
विज्ञान के क्षेत्र में जनसामान्य की भागीदारी बढ़ाने और वैज्ञानिक शिक्षा में सुधार द्वारा अधिक कुशल श्रमशक्ति के विकास में मदद मिलती है।
खगोल विज्ञान वैज्ञानिक शोध में वैचारिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस ज्ञान को मौसम, कम्प्यूटर विज्ञान, एवं संचार व्यवस्था जैसे प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।
खगोल विज्ञान वैज्ञानिक शोध में वैचारिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इससे अर्जित ज्ञान को मौसम विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, एवं संचार व्यवस्था जैसे प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्रों में आसानी से लागू किया जा सकता है। यह करने हेतु जिन उपकरणों की हमें आवश्यकता है वे महंगी भी नहीं है। यदि हम दूरसंवेदी डेटा से तुलना करें तो खगोल विज्ञान संबंधी डाटाबेस सस्ती भी हैं और सहज रूप से उपलब्ध भी हैं। तथापि आंकड़ों की प्रसंस्करण तकनीकें (मसलन, इमेज प्रोसेसिंग) दोनों ही मामलों में एक जैसी हैं।
अच्छी बात यह है कि विश्व में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों की सामुदायिक भावना ज्यादा मजबूत हैं एवं उनकी वैज्ञानिक दक्षताएँ ज्यादा हस्तांतरणीय हैं। उदाहरण के तौर पर होल अर्थ टेलीस्कोप (जो आंकड़ों का आदान-प्रदान एवं उनका विश्लेषण करने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगी मंच है) विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को अमरीका आमंत्रित करता है ताकि वे इस परियोजना के संस्थापकों के साथ काम कर सकें व उनसे सीख सकें।
ऐसी परियोजनाओं में विकासशील देशों के शोधकर्ता विश्व के कुछ चुनिंदा एवं सबसे उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन का हिस्सा बन सकते हैं और ऐसा करके विश्व के श्रेष्ठ शोधकर्ताओं के एक साझे मंच का विकास होता है। दरअसल वैश्विक सहयोग व नेटवर्किंग की संभावना खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है।
दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय परा-भौतिकी एवं खगोल विज्ञान कार्यक्रम (जो 11 विश्वविद्यालयों एवं 4 उन्नत शोध संस्थाओं का एक संयुक्त भागीदारी वाला मंच है जिसमें पीएचडी स्तर तक शिक्षार्थियों का प्रशिक्षित किया जाता है) पूरे देश का एक साझा कार्यक्रम है। इसके तहत पूरे अफ्रीकी महादेश के छात्र केपटाउन विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित होते हैं और इनमें से बहुत से वापस अपने देश में ऐसे खगोल विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बुनियाद रखते हैं।
ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था
हाल फिलहाल उन्नत विज्ञान पर औद्योगिक विश्व का एकाधिकार रहा है, परंतु खगोल विज्ञान उस ओर नई राहें बना रहा है।
ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था एवं वैज्ञानिक रूप से शिक्षित वैश्विक समुदाय के निर्माण के लिए विकासशील देशों की सरकारों का विज्ञान के मूलभूत विषयों पर कुछ हद तक निवेश करना आवश्यक है। दक्षिण अफ्रीका ने इसकी काफी पहले ही पहचान कर ली है। वहाँ की सरकार द्वारा 1996 में जारी एक श्वेतपत्र कहता है,
“पूरी दुनिया में जिज्ञासा आधारित विषयों पर शोध को आगे बढाने की एक प्रवृत्ति देखी गयी है जिसका सीधा फायदा होता है कि देश में प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि होती है…इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मूलभूत विषयों पर शोध को अव्यावहारिक न समझा जाए, क्योंकि यह उन यह मानकों के परिरक्षण करता है जिनके बिना प्रायोगिक विज्ञान का भी जीवन असंभव है।”
किसी भी देश द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में निवेश को सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि विकास हेतु उसके फ़ायदों को समझा जाए। दक्षिण अफ्रीका ने यह दिखा दिया है कि ऐसा करना संभव है। पूरे विश्व में फैले वेधशालाओं एवं खगोल विज्ञान से संबंधित संस्थाओं को चाहिए कि वे SCBP की तरह संस्थानों का विकास एवं समर्थन करें। खगोल विज्ञान से जुड़े समुदायों को मजबूती प्रदान कर विकासशील देश अपने विकास संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं।
साई-डेव पत्रिका में पूर्वप्रकाशित इस अंग्रेज़ी लेख का हिन्दी अनुवाद किया मिशिगन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक व हिन्दी चिट्ठाकार विजय ठाकुर ने। शुक्रिया विजय! अनुमति देने के लिये साई-डेव पत्रिका का भी आभार।