अपनी फिल्म के नायक, गंदी बस्ती में रहने वाला 18 साल का एक साहसी लड़का जो एक लोकप्रिय टीवी क्विज़ शो में 2 करोड़ रुपये जीतने कि कगार पर है, की ही तरह स्लमडॉग मिलियनेयर के रूप में डैनी बॉयल के हाथ तुरुप का पत्ता लग गया है।
स्लमडॉग पर क्या कहता है हिन्दी ब्लॉगमंडल
हिन्दी चिट्ठाजगत में स्लमडॉग के विषय पर दर्जनों पोस्ट लिखी गई हैं पर बहुत कम लोगों ने ही फिल्म देखने के बाद इसकी समीक्षा लिखी। कुछ लोगों को फिल्म के शीर्षक में “डॉग” शब्द के प्रयोग पर ज़्यादा आपत्ति है और शेष ने कहेसुने के आधार पर अपनी राय लिखी। सामयिकी ने हिन्दी ब्लॉगमंडल का एक चक्कर लगाया और जो स्वर मिले उन्हें आप तक पहुंचा रहे हैं
दिल कड़ा कर के जाना होगा हॉल में
अमरीकी सिनेदर्शकों से भरे हॉल में ऐसा लगा जैसे हमें पश्चिम वालों के सामने नंगा किया जा रहा है…फिल्म में रोमांच है, रोमान्स है, बढ़िया अदायगी है। सब अच्छा है, बस केवल यही अच्छा नहीं लगता कि हॉलीवुड को भारत का अच्छा पहलू दिखाने में क्या दिक्कत है। – रमण कौल

Cartoon by Kirtish Bhatt
समस्या स्लम से है, डॉग से, या उसे मिलेनियर बनाने वाले से?
बजाय मिलेनियर बनाने वाले को गरियाने के अगर हम स्लम बनाने वालों को गरियाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। – तरुण
स्लमडॉग मिलियनर – झुग्गी का कुत्ता, 10 लाख वाला
मेरा प्रश्न ये है कि कैसे कोई इंसान दूसरे इंसान को कुत्ता कह देता है। और ये अंडरडॉग की तरह एक मुहावरा नहीं है, गाली है, हिकारत है, संवेदना रहित शाब्दिक दिवालियापन है। – हरि प्रसाद शर्मा
गाली, जो पुरस्कार के बोझ तले दब गई!
एक विदेशी को इस तरह के नाम वाली फिल्म की शूटिंग हमारे देश में करने क्यो दी गई? इसके अधिकतर किरदारों के मुस्लिम नाम है ! क्या यह मुसलमानों को नीचा दिखाने और दुनिया के मुसलमानों के दिल में यह नफरत पैदा करने के उद्देश्य से तो नही बनाई गई कि इस देश में यें लोग कितनी दयनीय स्थिति है? – PCG
मेहनतकश स्लम डॉग ही असली मिलेनियर
फ़िल्म बेहतरीन हैं लेकिन वो भी कहीं न कहीं युवा वर्ग के मन में फ़ेन्टेसी लैन्ड बना देती हैं। मेरी नज़रों में पटना के सुपर 30 में पढ़ाई कर आईआईटी तक पहुंचे बच्चे या फिर मेहनतकश स्लमडॉग ही असली मिलेनियर हैं। – अशोक दुबे
आस्कर ही श्रेष्ठता का प्रमाण क्यों?
युरोप में एक ऐसा वर्ग विकसित हुआ है जो भारत को विश्व पटल पर दरिद्र व भ्रष्ट देश दिखाना चाहता है इसीलिए यह वर्ग इन यूरो-इंडियन की घिनोनी मानसिकता को मेगसेसे व बूकर पुरस्कार देकर पोषित करता है…यदि आप टेक्नालोजी को छोड़ दे तो अन्य किसी मामले में हम हॉलीवुड से पीछे नहीं है, परन्तु जाने क्यों हमने आस्कर को ही श्रेष्टता का प्रमाण मान लिया है। – सुनील सयाल
मंच पर तालियों से कुछ बदलेगा नहीं
सच्ची कलाकारी तो इस बात में है कि आप भूखी-नंगी जनता के लिए कुछ भी कर पायें। … नहीं तो आपकी कलाकारी गई चूल्हे में, उन्हीं कुत्तों की बला से, जिनका चित्रण आपने “स्लमडॉग” में किया है!! भइया इस तरह के चित्रण को कर के दुनिया के तमाम फिल्मी मंचों पर तालियाँ अवश्य बटोरी जा सकती है मगर उससे कुछ भी बदल नहीं पाता!! – राजीव थेपडा
संकलनः रमण कौल
और जमाल की ही तरह, जिस पर किसी को यकीन नहीं होता कि वो टीवी शो पर बिना धोखाधड़ी के इतनी आगे तक जा सकता है, बॉयल के लिए भी कुछ आलोचकों ने कहा कि उन्होंने एक आसान शार्टकट पकड़ा है और गरीबी का “इस्तेमाल” कर ‘हम गरीब हैं पर हम खुश हैं’ नुमा कहानी को भुनाया है।
चार अमरीकी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने और ब्रिटेन व अमेरिका के बॉक्स आफिस पर अब तक करीब 5 करोड़ डॉलर कमाने के बाद स्लमडॉग निःसंदेह चारों ओर चर्चा का विषय बनी हुई है।
हर तरह तारीफें बटोर रही व चर्चित मिश्रित कास्ट वाली यह फिल्म व्यग्र और अतिश्योक्तिपूर्ण महानगर मुंबई और दुनिया की सबसे उर्वर फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के प्रति बॉयल का स्तुतिगान भी है।
फिल्म में शहर की घुटनभरी और रंगीन गंदगी और इसमें में रह रहे लोगों के चित्रण पर कुछ लोगों ने इसे मुंबई पर डिकॅन्स का नज़रिया बताया है। तो कुछ लोगों ने इस पर व्यंग्य कसते हुए इसे गरीबी का घासलेटी साहित्य करार दिया है। एक आलोचक ने बॉयल के काम को ”फैशनेबल गंदी बस्ती (Slum Chic)” कहा।
बात सही है, कूड़े-कचरे के पहाड़ों की छांव में, सांप्रदायिक दंगों में बच्चों के सामने उनकी मांएं कत्ल कर दी जाती हैं और फिल्मी स्टार से प्रभावित गंदी बस्ती का एक लड़का खुले आसमान के नीचे शौच करते हुए मल के कीचड़ में गिर जाता है। एसिड से बच्चों की आखें जला दी जाती हैं, और लंपट नौजवां लड़कियों को जबरन वेश्यालयों में धकेल देते हैं।
भारत में फिल्म के रिलीज होने के एक दिन पहले, कुछ एनजीओज़ ने खबरचियों को “असली स्लमडॉग्स” से मिलने का आमंत्रण दिया। मेरे इनबॉक्स में पड़े एक आमंत्रण पत्र में लिखा है, “हम आपके दिल्ली की गंदी बस्तियों में जाने और असली स्लमडॉग्स से इंटरव्यू लेने का मौका दिला सकते हैं – ऐसे बच्चे जो हर रोज असीम गरीबी में जीते हैं”।
अन्य अनेक चीजों की तरह, मुक्त बाजार में गरीबी भी एक अच्छा व्यापार है। पर भारत गरीब लोगों के लिए बेहद क्रूर और बच्चों के प्रति कठोर भी है, और दुनिया के सबसे ज्यादा असमान समाज में से एक है।
मुझे बॉयल की फिल्म में गंदी बस्ती में रहनेवाले बच्चों की सहनशक्ति और गंदी बस्ती के जीवन की अच्छाईयों के चित्रण से कोई परेशानी नहीं है: ये तो कभी न बदलने वाले लोकप्रिय पूर्वी रूढ़िवादी धारणा का हिस्सा है, गरीब यानि गंदी बस्ती यानि गंदे, मुस्कुराते बच्चे। हम इन बातों से बखूबी वाकिफ़ हैं।
दरअसल, ऐसा लगता है कि भारतीयों ने भी पश्चिमी फिल्मकारों द्वारा भारत की बेबस गरीबी की निर्मित छवि को स्वीकार लिया है।
मुझे वो सेट याद हैं – एक बड़ी गंदी बस्ती, और क्या हो सकता था? पैट्रिक स्वेज़ी अभिनित रॉलैंड जॉफ की करोड़ों की लागत वाले सिटी ऑफ जॉय के सेट, जिसे 1990 में कलकत्ता में लोगों ने जला दिया गया। उनका आरोप था की वे गरीबी बेच रहे हैं। जॉफ को अपना सामान बांध कर शहर छोड़ना पड़ा। फिल्म को बाद में लंदन के पाइनवुड स्टूडियो में पूरा किया गया।
स्लमडॉग मिलियनेयर को लेकर मेरे सवाल कुछ और हैं। ये फिल्म मुझे प्रभावित नहीं कर पाई।
मुझे लगता है कि बॉयल एक बॉलीवुड फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे – बिछड़े गरीब भाई, एक तरफा प्यार – और उस पर वास्तविकता का ढेर सारा तड़का। पर अंततः ये उस शैली की एक अपरिपक्व नकल है जिसे सिर्फ भारतीय ही उस उत्साह व आवेग से बना सकते हैं जिसकी वह हकदार है।
फिल्म में वास्तविकता बस सतही है, और कुछ शानदार अभिनय के बावजूद कथानक पर स्टाईल हावी रहता है। और फिल्म मुझे उस तरह से बांधे नहीं रख पाती जैसा की, मसलन, 2002 में बनी रिओ डे जनेरो के फवेलास में ज़िंदगी की कहानी बताती ब्राज़ीलियाई अपराध नाटिका “सिटी आफ गॉड”।
शानदार संपादन और चपल छायांकन की बदौलत स्लमडॉग के दृश्यों की तेज़ गति अचंभित करती है। ये भड़कीली है, पर उतनी भी नहीं कि बॉलीवुड से टक्कर ले सके। रेल्वे स्टेशन पर एक नृ्त्य एरोबिक की कक्षा नुमा लगता है। फिल्म का साउंडट्रैक रैप, हिपहॉप और फंक बॉलीवुड की शोरगुल भरी खिचड़ी है। ए आर रहमान गोल्डन ग्लोब के हकदार हैं पर स्लमडॉग बिलाशक उनका श्रेष्टतम कार्य नहीं है।
हर किसी को एक शोषित की कहानी अच्छी लगती है। शायद इसलिए इस निराशाजनक दौर में स्लमडॉग दर्शकों के दिलों को छू गई। पर चतुराई से कहानी बयाँ करने की कला से इसके घिसापिटे होने की बात छिप नहीं सकती।
अन्य अनेक फिल्मों की तरह स्लमडॉग भी ये साबित करती है कि वैश्विकरण के बावजूद संस्कृतियाँ एक दूसरे को समझने में काफी हद तक नाकाम रही हैं। चूंकि भारतीय सिनेमा पश्चिम में बहुत लोगों के लिए एक बेकार बॉलीवुड मेले का द्योतक है, आलोचकों से सराहना प्राप्त, और अक्सर लोकप्रिय, फिल्मों, जिनमें भारत के दबेकुचलों को किसी विदेशी फिल्म से ज्यादा उग्र व ओजस्विता से पेश किया गया है, को नियमित रुप से नजरअंदाज कर दिया जाता है।
आपको सत्यजीत रे याद हैं? भारत के एकमात्र आस्कर जीतने वाले फिल्मकार जिनका “गरीबी बेचनेवाले” के रुप में अपने देश में ही उपहास होता था और जिनका शुरुआती काम अकाल पीड़ित भारतीय गांवों पर आधारित था? भारत-विभाजन के बाद कलकत्ता के झोंपड़ पट्टियों में आतंक का दिल दहला देनेवाला चित्रण करने वाले रित्विक घटक याद हैं? और हाल की बात की जाय तो कुछ युवा भारतीय फिल्मकारों ने ऐसे विषयों पर काम किया जिनमें भारत की कई बगावतें और कमजोरियाँ उजागर होती हैं।
स्लमडॉग मिलियनेयर से जो सबक मिलता है वो यह है कि “बॉलीवुड” की शैली पूरी तरह भारत की ही है और किसी की नहीं, और कोई भी इस शैली में हमसे बेहतर फिल्म नहीं बना सकता।
और अगर आप मुंबई के गंदले इलाकों की साहसिक वास्तविकता देखना चाहते हैं तो रामगोपाल वर्मा की फिल्म सत्या की डीवीडी ले आइए। 1998 में मुंबई के रंगीले अंडरवर्ल्ड में मजबूरन शामिल आप्रवासियों पर बनी इस फीचर फिल्म के मुकाबले स्लमडॉग एक चतुर, उत्साहजनक एमटीवी डाक्यू-ड्रामा लगती है।
बीबीसी पर प्रकाशित लेख का पूर्वानुमति से अनुवाद। सौतिक के लेख का अनुवाद किया है पूर्णिमा शर्मा ने। पूर्णिमा दिल्ली आजतक, डीडी न्यूज़ व पल्स मीडिया के साथ काम कर चुकी हैं। संप्रति हिंदुस्तान टाईम्स समूह के दैनिक अखबार के लिये फ्रीलांसर के रूप में काम कर रही हैं। उनसे संपर्क का पता है sharmapurnima1 at gmail dot com।











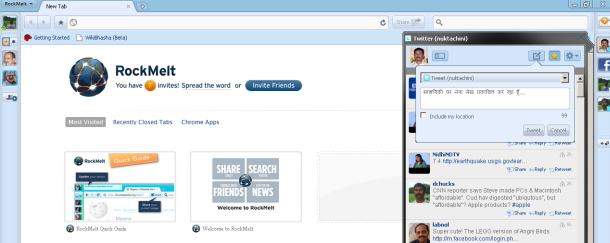
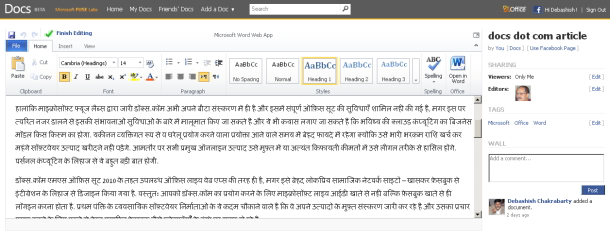
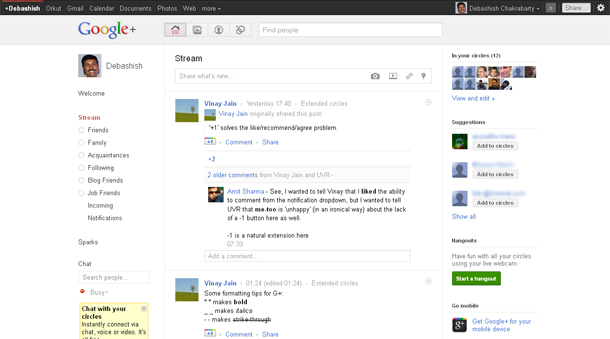
अनुवाद और प्रस्तुति (बाजू पट्टी में हिन्दी ब्लॉगजगत की राय) दोनों ही जानदार.
…. ‘हम गरीब हैं पर हम खुश हैं’ शायद यह सच है … लेकिन सच नहीं है. समीक्षा अच्छी लिखी पर क्या गैरजरूरी नहीं… महज एक फिल्म के लिए? यह बॉयल के काम से किस तरह अलग है? बहरहाल मुझे आपके प्रस्तुतिकरण ने प्रभावित किया.
बहुत बढ़िया लेख है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
[…] box-item at Hindi version of Slumdog Millionaire BBC Review at […]
क्यूँ मुझे ये लेख प्रभावित नही कर पाया
मुझे पता नही क्यूँ ऐसा लगा शायद जिसने भी ये लेख लिखा originaly,दिमाग पे बहुत कुछ बोझा ढोए हुए हो जैसे या फ़िर बहुत sare Reviews पढ़ के लेखा हो …
ये लिखना “अन्य अनेक फिल्मों की तरह स्लमडॉग भी ये साबित करती है कि वैश्विकरण के बावजूद संस्कृतियाँ एक दूसरे को समझने में काफी हद तक नाकाम रही हैं” बिल्कुल भी सही नही है …सच बोलूं तो मुझे ही बहुत sari नयी चीजे पता चली स्लम के बारे मैं …
Overall this movie gave me one new perspective about my country which we can only appreciate if we see this movie with an open mind and that’s the difficult thing!!
Regards
Divya Prakash Dubey
[…] articles (Hindi): Slumdog Millionaire Review, Box item on BBC review on Samayiki Tags: Anil Kapoor, Bollywood, Hollywood, Oscar, Slumdog […]